कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दृष्टि में
Hello दोस्तों ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर स्वागत है । आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक नया Topic जिसमें हम समझेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में । इन्हें लोकतंत्र का स्तम्भ भी कहा जाता है, जिसके कारण देश को चलाया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाये जाते है, और उन्हें लागू किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं ।
राजनीति विज्ञान में अक्सर हम इन शब्दों को पढ़ते हैं । संविधान में भी यह शब्द आते रहते हैं । तो इन शब्दों को किस तरीके से समझें ? कैसे इनका विश्लेषण करें ?
सबसे पहले भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और संविधान बनाया गया । सुचारू रूप से उसमें तीन तरह से कार्य करने वाले 3 अंग बनाए गए । एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका । आइये इनको Detail में समझते हैं ।
कार्यपालिका का अर्थ
सबसे पहले कार्यपालिका और उसके कार्यों के बारे में जानते हैं । व्यक्तियों का समूह जो कायदे कानून को लागू करवाता है, कार्यपालिका कहलाता है । कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, जो विधायिका द्वारा बनाये कानून को लागू करता है, तो भारत में विधि या किसी भी तरीके का कानून बनाने का काम विधायिका का होता है । कोई भी बिल बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और इस बिल को लागू करने (Power of Execute) की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है ।
राष्ट्रपति की शक्तियों और निर्वाचन प्रणाली के बारे में जानने के लिए यहाँ Click करें ।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के लिए यहाँ Click करें ।
बिल बनाना, उसे लागू करना, कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है । और अगर इसे लागू करने में कोई समस्या आती है तो यानी कोई न्यायिक चुनौती आती है या फिर कोई उल्लंघन करता है । तो उसकी सजा का प्रावधान यानी न्याय की व्यवस्था की शक्ति, न्यायपालिका के पास होती है ।
न्यायिक सक्रियता पढ़ने के लिए यहाँ Click करें ।
तो इससे यह समझ में आता है कि कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है । कानून को लागू कराने की ताकत कार्यपालिका के पास होती है और उसके उल्लंघन के मामले में सजा देने की प्रवधान न्यायपालिका को प्राप्त है ।
कार्यपालिका के अंग
सबसे पहले हम कार्यपालिका के अंगों के बारे में जानते हैं । कार्यपालिका जो कार्य को चलाती है, उसमें 2 स्तर पर सरकारें बनाई जाती हैं ।
एक केंद्र स्तर पर और
दूसरी राज्य स्तर पर
कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर कौन-कौन होता है और राज्य स्तर पर कौन-कौन आता है । आइये समझते हैं । तो जो केंद्र स्तर पर सरकार बनाई जाती है ।
कार्यपालिका में राष्ट्रपति, केंद्र स्तर पर सबसे प्रमुख होता है । कार्यपालिका में राष्ट्रपति ना केवल केंद्र स्तर पर बल्कि पूरे भारत में महत्वपूर्ण पद है, जो एक मुखिया (Head) माना जाता है । दूसरे महत्वपूर्ण रूप में आते हैं, उपराष्ट्रपति और कार्यपालिका में तीसरे नम्बर पे आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री । और प्रधानमंत्री को वास्तविक मुखिया (Head) कहां जाता है |
लोकतंत्र क्या है ? (Introduction of Democracy) जानने के लिए यहां Click करें ।
हालांकि भारत में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई है । लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है । इसलिए इन्हें कार्यपालिका की नामित शक्ति, कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति का हकदार माना जाता है ।
और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है, मंत्री परिषद ।
तो यह सभी केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं ।
मंत्री परिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं ।
कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री
उप मंत्री
यह तीनों मंत्री कार्यपालिका के अंग होते हैं ।
कार्यपालिका को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा जा सकता है ।
1 स्थायी और
2 अस्थायी
स्थायी
स्थायी कार्यपालिका में वह सदस्य आते हैं जो, लंबे समय के लिए स्थायी (Permanent) रूप से चुने जाते हैं । इनके कार्यकाल की अवधि 60 या 62 साल तक की आयु के लिए होती है । जैसे आईएएस (IAS) अधिकारी आदि ।
अस्थायी
इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद आदि, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं । तो यह अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं ।
केंद्र के समान दोस्तों यहां राज्य में भी कार्यपालिका होती है और राज्य में हम देख सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति आते हैं ।
राज्यपाल
मुख्यमंत्री
मंत्री परिषद
स्थायी कार्यपालिका दोनों जगह केंद्र और राज्य में होती हैं और इनमें वह अधिकारीगण होते हैं । जो अधिकारी के रूप में अपनी सेवा देते हैं । सचिव के पद पर होते हैं । यह सब स्थायी कार्यपालिका के अंदर होते हैं ।
कार्यपालिका को समझने के लिए इसकी पूरी Detail में पढ़ना होगा । इस में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के बारे में detail में दिया गया है । इनके कार्य क्षेत्र क्या हैं ? क्या शक्तियां है ? क्या दायित्व हैं ? आदि । इनको अलग से बताया गया है ।
विधायिका
अब बात करते हैं, विधायिका की । विधायिका का मतलब यह होता है विधेयक (Bill) बनाना । इसमें विधेयक बनाने संबंधी कार्य किये जाते हैं । विधायिका को भी केंद और राज्य दो स्तर पर बांटा जाता है ।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूचियों के बारे में । सूचियां तीन प्रकार की होती हैं । राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची ।
जो केंद्र सूची है । वह उन विषयों पर जब विधि बनाने की बात आती है । वह केंद्र द्वारा बनाई जाती है । जो राज्य सूची का विषय है । वह कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और समवर्ती सूची वह है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं ।
अब यह जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर विधायिका काम करता है । उनका मुख्य काम होता है, विधि बनाना । विधि बनाने के लिए केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था है की गई है । उसका नाम है,
संसद और
जो राज्य स्तर पर जो व्यवस्था है । उसका नाम है,
विधान मंडल ।
अब केंद्र में कानून बनाने के लिए इस संसद के दो अंग होते हैं ।
लोकसभा और
राज्यसभा
और यह दोनों सदन मिलकर के कोई भी विधेयक तैयार करते हैं ।
और इसी सदन के सदस्य को हम विधायिका कहते हैं । वास्तव में उन्हें सांसद कहा जाता है । MP (Member of Parliament) यह विधायिका का अंग होते हैं और यह विधेयक बनाते हैं ।
जब राज्य स्तर पर आते हैं । तो विधानमंडल में भी दो स्तर आते हैं । इसमें आप देखेंगे
विधानसभा और देखेंगे
विधान परिषद ।
विधानसभा सभी राज्य में अनिवार्य होती है । विधान परिषद सभी राज्य में अनिवार्य नहीं होती या यह निर्भर करता है कि उस राज्य पर की विधान परिषद रखना चाहते हैं या नहीं । यह विधान परिषद रखने वाले राज्यों की वर्तमान में संख्या 7 है । अगर राज्य चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं और राज्य से रख भी सकते है । तो यह चलता रहता है, तो इस तरह से राज्य स्तर पर विधानमंडल, विधान सभा का काम करते हैं ।
प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने के नाते, वह विधायिका के भी अंग होते हैं और जब कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगते हैं । तो कार्यपालिका के भी अंग होते हैं । उसी तरह से जितने भी मंत्री पद होते हैं । जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, तो जितने भी मंत्री बनते हैं । यह मंत्री बनने के बाद कार्यपालिका के अंग बन जाते हैं और जब तक मंत्री नहीं है । वह विधायिका का अंग रहते हैं । तो एक ही व्यक्ति कार्यपालिक भी हो सकता है और विधायिका भी हो सकता है । उसी समय जब वे संसद में बिल पास करने जाता है । तो विधायिका के रूप में काम करता है और जब वह अपने मंत्रालय में रहते हुए कार्य करता है, तो उस समय वह कार्यपालिका का अंग होता है ।
तो इस तरह से विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी सदस्य हो सकते हैं । यह हमेशा याद रखें विधायिका और कार्यपालिका में आपस में अनुबंधित (Bonding) है ।
न्यायपालिका
अब बात करते हैं न्यायपालिका की ।
कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर कानून का कोई उल्लंघन न करे, इसे रोकने के लिए । दोषियों को दंड के प्रावधान के लिए आमतौर पर न्यायपालिका की बात की जाती है ।
भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और उसे एकीकृत रूप में डाला गया है । यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक श्रृंखलाबद्ध रूप में उसको बनाया गया है । इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं । जैसे हमारे यहां सबसे ऊपरी स्तर पर जो न्यायालय है, वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फिर उसके निचले स्तर पर हाई कोर्ट ( High Court) फिर उसके निचले स्तर पर आते हैं । तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (District Courts) या सत्र न्यायालय । इस तरीके से यह न्यायपालिका का एक क्रमिक चरणबद्ध श्रंखला है । जिसे हम एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं ।
न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका की तरह केंद्रीय और राज्य स्तर पर नहीं बांटा जा सकता । इसमें ऐसा नहीं होता कि केंद्र का सुप्रीम कोर्ट या राज्य का हाईकोर्ट है । इसका यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि कोई न्यायालय राज्य का है या केंद्र का है । वास्तव में यह एक क्रमिक श्रृंखला है । जिसमें विधिवत रूप से यदि कोई किसी कोर्ट के फैसले को नहीं मानता हैं तो वह उसके ऊपर के कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं । यानी कोई व्यक्ति कोर्ट के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके उच्च कोर्ट में जा सकता है ।
अनुच्छेद 50 के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसमें, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण है । यहां पर विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़कर काम करती हैं, मिलकर काम करते हैं । लेकिन इसमें यह बताया गया है, कौन से स्थिति में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया है । क्यों रखना चाहिए ? यदि सरकार और जज, दोनों एक दूसरे से सांठगांठ रखेंगे तो, किसी भी कीमत पर निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा । इस तरह की स्थिति में न्यायपालिका सरकार पर किसी परिस्थिति में अच्छे काम करने के लिए दबाव बना पाएगी । तो इसलिए अगर यह दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहकर काम करते हैं । तो जनता की भलाई अधिक हो पाती है और जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं । संविधान में है वह पूरा हो जाता है । इसलिए अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग अलग होने की बात कही गई है ।
यह एक क्रमिक श्रृंखला में काम करते हैं और सबके काम एक दूसरे का सहयोग करना है ।
यह तीनों स्तंभ मिलकर एक भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बनते हैं । कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका । हमारा लोकतंत्र इन तीनों स्तंभों पर टिका हुआ है ।
मीडिया (माध्यम)
और आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है । क्योंकि वर्तमान में मीडिया का लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है । वर्तमान में लोगो को मीडिया के माध्यम से ही सरकार की नीतियों का पता चलता है । टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, मैगज़ीन आदि से पक्ष और विपक्ष के बारे में विश्लेषण किया जाता है । विशेष योग्यता वाले व्यक्ति मीडिया के द्वारा अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं ।
तो दोस्तो अगर यर Post आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ Share करें । तब तक के लिए धन्यवाद !!


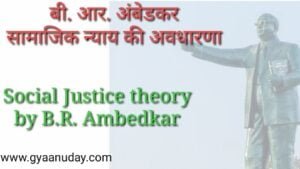

Pingback: शक्ति का पृथकीकरण सिद्धांत – Gyaan Uday